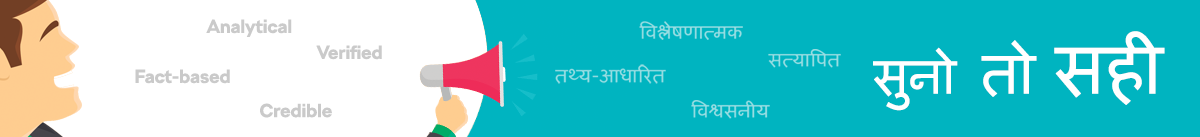यह समय कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणामों का है और समाचार पत्र छात्र-छात्राओं की तस्वीरों से भरे हुए हैं। यह देखना वास्तव में अच्छा है कि इतने सारे बच्चों ने इतने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन यह समय शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण नज़र डालने का भी है।
आज से कुछ दशक पहले, प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत या उससे अधिक) प्राप्त करना एक उपलब्धि माना जाता था। तो फिर पिछले दशकों में ऐसा क्या बदल गया? क्या वर्तमान पीढ़ी के बच्चे पहले की पीढ़ियों के बच्चों की तुलना में अत्यधिक तेज हो गए हैं?
2016 में मुझे सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता का पद मिला, और तब मुझे ज़मीनी हकीक़त का सामना करना पड़ा। जिस तरह की चीज़ें सुन ने में आ रही थी, उनपर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। छानबीन करने पर पता चला कि मॉडरेशन के नाम पर कई बोर्ड बच्चों को मार्क्स बहुत बढ़ा कर दे रहे थे। बच्चों को मार्क्स बढ़ा कर देने का ये सिलसिला 10 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्रों को पास करने के लिए अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क्स) प्रदान करने के साथ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे यह बोर्ड परीक्षार्थियों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों (मुख्य रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय) में प्रवेश दिलाने का एक तरीका बन गया।
लगभग हर छात्र को जितना उन्हें मिलना चाहिए उससे 10 प्रतिशत ज़्यादा अंक मिलने लगे। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में बड़ी संख्या में छात्रों ने 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, क्योंकि 95 प्रतिशत बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा (स्पाईकिंग सीलिंग) है जिसके आगे अंक नहीं बढ़ा सकते। प्रभावी रूप से 85 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच स्कोर करने वाले सभी छात्र 95 प्रतिशत प्राप्त करने लगे। इससे बड़ा तमाशा और क्या हो सकता है! कुछ अन्य बोर्डों में, मार्क्स बढ़ाने की सीमा 100 प्रतिशत थी। इसके परिणामस्वरूप छात्रों को भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में भी 100 प्रतिशत मिलने लगे। भारत में इस स्थिति को गंभीर नहीं माना गया क्योंकि वर्तमान में भविष्य की कीमत पर लाभ हो रहा था।
इन सब के बावजूद भी, CBSE (कक्षा 12) में पूरे भारत का उत्तीर्ण प्रतिशत 88 प्रतिशत था, जो हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक प्रश्नचिन्ह है। उत्तीर्ण प्रतिशत काफी हद तक कम हो गया होता, अगर इस तरह से अंक बढ़ाकर नहीं दिए जाते। लेकिन तथ्यों का सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक राज्य बोर्ड के अध्यक्ष ने जब यह सब बंद करने की कोशिश की तो उनको हटा दिया गया।
इस भ्रम से सभी खुश थे। छात्र खुश था क्योंकि उसे अधिक अंक मिल रहा था। वह इस बात से जानबूझ कर अनजान था कि उसने यह अंक अर्जित नहीं किये हैं। शिक्षक खुश था, क्योंकि औसतन, हर बच्चे ने अधिक स्कोर किया। स्कूल डिस्टिंक्शन का दावा कर सकता था भले ही यह वास्तव में मौजूद न हो। सरकारें खुश थीं क्योंकि लोगों की नज़र में राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहा था।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दौरे (शुरुआती कुछ महीनों में 21) के समय, इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। लगभग हर कोई इस बात से सहमत था कि इस को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन वे इसे जारी रखने के लिए मजबूर थे क्योंकि बाकी लोग इसे जारी रखना चाहते थे।
कुछ राज्य सरकारों ने मॉडरेशन के नाम पर अंकों को बढ़ाना बंद किया और कर्नाटक में पास प्रतिशत में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आ गयी। पंजाब में भी पास प्रतिशत 10 प्रतिशत से अधिक गिर गया। कई अन्य राज्यों ने भी अंक बढ़ाने की बजाय सच्चाई का सामना करना चुना।
सीबीएसई भी अब अंक बढ़ाने की प्रक्रिया को बंद करने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन दिल्ली में रहने वाले प्रभावशाली माता-पिता जैसे राजनेता, सिविल सेवक और अधिवक्ता उच्च प्रतिशत के भ्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मीडिया भी इस सब में शामिल हो गया और इच्छुक पार्टियों ने आधी-अधूरी बातें बताने में कामयाबी हासिल कर ली। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अंकों का मॉडरेशन उस तरह से जारी रहना चाहिए जैसा कि पिछले वर्षों के दौरान किया गया था। आदेश में अंकों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने (ग्रेड स्पाईकिंग) का कोई उल्लेख ही नहीं था। सीबीएसई ने मंत्रालय के निर्देश पर आदेशों का पालन करना चुना। हर कोई खुश था क्योंकि पास प्रतिशत नहीं गिरा।
जो भी कारण हो, अंकों के साथ छेड़छाड़ परीक्षा प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को मिटा देती है और मूल्यांकन पैटर्न की विश्वसनीयता को कम करती है। यह जानबूझकर बच्चों को उनके सीखने के स्तर के बारे में गलत संकेत देता है और आगे जाकर इन्ही बच्चों को जब प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होता है तो उन्हें एक भावनात्मक गिरावट का सामना करना पड़ता है।