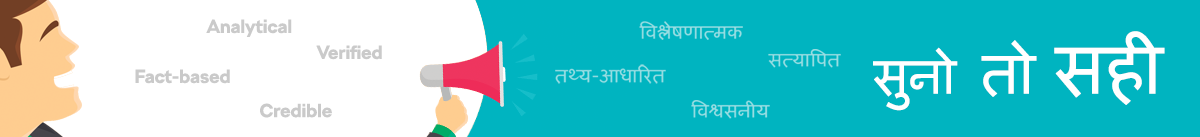रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिनांक 8 मई को धारचूला-लिपुलेख (भारत-चीन सीमा) मार्ग के उद्धघाटन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी देश नेपाल द्वारा यह दावा पेश किया गया है कि उक्त मार्ग उसके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र से होकर गुज़रता है।यह सड़क परंपरागत कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा पथ का अनुगमन करती है। यह एक कठिन रास्ता है, जिस पर मैंने स्वयं सन 1981 में सफर तय किया था। यह वह वर्ष था जब भारत चीन समझौते के तहत यात्रा मार्ग को 25 वर्षों के समय के पश्चात, लिपुलेख मार्ग के ज़रिए पुनःआरंभ किया गया था। ट्रैकिंग के रास्ते का एक पक्की सड़क में परिवर्तित होना तीर्थयात्री व व्यापारियों, दोनों के ही लिए यह किसी वरदान से कम नही है।
नेपाल द्वारा किये गए दावे की व्याख्या
वर्तमान विवाद की स्थिति ने नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को अपनी सरकार के नेपाल की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा न कर पाने की असफलता व अक्षमता को छिपाने का एक अवसर प्रदान कर दिया है। साथ ही उन्हें इसमें अपनी स्वयं की पार्टी से उनके निरंतर बढ़ते विरोध से सभी का ध्यान हटाने का भी अवसर प्राप्त हो गया है। उनके द्वारा नेपाली संसद में दिए गए असंयमी कथनों को भारत-नेपाल के रिश्तों को संरक्षित करने के हित में नज़रअंदाज़ करना ही बेहतर होगा।
नेपाल द्वारा अपनी सशस्त्र पुलिस सेना को छारुंग (Chharung), कालापानी के निकट, अपने सुदूर पश्चिम में तैनात किया गया । हालांकि, सेना की की गयी तैनाती में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन उसके तरीके एवं समय-चयन ने नई दिल्ली के समक्ष कईं अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल भी, चीनी सीमा के नज़दीक होने की वजह से, कालापानी में ही स्थित है। भारतीय सेना वहाँ नेपाल की वजह से नही मौजूद है।
नेपाली सरकार ने एक नए नक्शे को, जिसमे नेपाल की सीमा उन क्षेत्रों में पहुँच जाती है, जो भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अधिकृत कर उक्त स्थिति के निराकरण को और अधिक जटिल बना दिया है।
सुगौली संधि
सीमा रूपरेखा का इतिहास काफ़ी पुराना है। सन 1816 की सुगौली संधि के पहले नेपाली राज्य की सीमाएं पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूरब में तीस्ता नदी तक स्थित थीं। नेपाल को एंग्लो-नेपाली युद्ध में हार का सामना करना पड़ा जिसके कारणवश उक्त संधि ने नेपाल की सीमाओं को आज के परिदेश्य में सीमित कर दिया। सुगौली संधि के अनुसार “नेपाल के राजा द्वारा सम्माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी को अनंत काल के लिए उक्त भूखंड सौंपा जाता है”, जिसमे “नदी काली एवं नदी राप्ती के बीच की समतल नीच भूमि” शामिल है। संधि में आगे यह भी लिखा गया था कि “नेपाल के राजा, उनके वारिस व उत्तराधिकारी, काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी क्षेत्रों व वहाँ की जनता से अपने सभी अधिकारों का त्याग करते हैं”।
मौजूदा विवाद के उत्पत्ति का कारण है नेपाल का यह दावा कि वह सहायक नदी जो कालापानी में महाकाली नदी से मिलती है वह काली नदी नहीं है। अब नेपाल का यह दावा भी है कि काली नदी लिपुलेख दर्रे से भी आगे पश्चिम दिशा में स्थित है।अंग्रेज़ों द्वारा लिपुलेख दर्रे का उपयोग तिब्बत व चीन के साथ व्यापार के लिए किया जाता था। भारतीय सर्वेक्षण अभियान द्वारा सन 1870 के दशक से लिपुलेख दर्रे से कालापानी तक के इलाके को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बताया गया। नेपाल के राणा शासक व नेपाली राजाओं द्वारा भी उक्त सीमा को पूर्ण रूप से मान लिया गया था व 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी उनके द्वारा कोई आपत्ति इस पर नहीं उठायी गयी।
सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों को जंग बहादुर राणा द्वारा दी गयी सैन्य मदद के पुरस्कार स्वरूप नेपालगंज व कपिलवस्तु के इलाकों को नेपाल में पुनःस्थापित कर दिया गया था। किन्तु अंग्रेज़ों द्वारा गढ़वाल अथवा कुमाऊं (कालापानी क्षेत्र को शामिल करते हुए) के किसी भी क्षेत्र को नेपाल को नहीं दिया गया था।
सन 1816 में, जब सगौली संधि निर्धारित की गयी थी, तब भारत अस्तित्व में नहीं था। और वर्तमान में, नेपाल ही नही, बल्कि अन्य कईं पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाएँ तत्कालीन अंग्रेज़ हुकूमत द्वारा बनायी गयी थीं। भारत ने इन सीमाओं को अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद प्राप्त किया। अब ऐसे ऐतिहासिक अतीत को पूर्ववत नहीं किया जा सकता।
समाधान की ओर
सन 1981 में सीमा से संबंधित मामलों का हल खोजने, अंतरराष्ट्रीय सीमा व सीमा स्तम्भ निर्धारित करने के लिये भारत-नेपाल तकनीकी स्तरीय संयुक्त सीमा कार्यकारिणी दल का गठन किया गया था। 2007 तक इस दल द्वारा 182 नक्शे पट्टियों को तैयार कर लिया गया था, जिन्हें दोनो पक्षों के सर्वेक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित भी कर लिया गया था। उक्त पट्टियों में लगभग 98% क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था, लेकिन इनमें दो विवादित क्षेत्र, कालापानी और सुस्ता को बाहर रखा गया।
इनके अलावा बचे हुए सीमा संबंधित समस्याओं को सुलझाना कठिन नही होगा ,यदि वे घरेलू अथवा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में नहीं उलझे हुए हों। संबंधित सरकारों द्वारा उक्त नक्शों का अनुमोदन करना (जो कि नेपाल सरकार द्वारा किया जाना शेष है), कालापानी व सुस्ता से संबंधित मतभेदों का निराकरण व गुम हुए अथवा क्षतिग्रस्त सीमा स्तंभो का शीघ्रता से लगाना अगले कदमों में शामिल है।
भारत द्वारा कुछ समय पहले ही काफ़ी कठिन लगने वाले हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, ज़मीन व समुद्री सीमा विवादों को सुलझाया जा चुका है। ज़मीनी सीमा के मामले में कुछ प्रतिकूल कब्ज़े वाले भूखंडों का विनिमय व जनसंख्या का स्थानांतरण भी शामिल था, और इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक भी पारित किया गया जिसने सन 1974 के भारत-बांग्लादेश समझौते को प्रभाव दिया। समुद्री सीमा से संबंधित मामले को सुलझाना और भी अधिक जटिल था। भारत ने हेग में स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मामले को लेकर जाने की अपनी सहमति दी, यह जानते हुए कि यदि कोर्ट द्वारा इस मामले को न्यायसम्यता के आधार पर सुना, तो भारत को लगभग चार चौथाई हिस्से को बांग्लादेश को देना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपने दावे को आधार रेखा पर आधारित किया था, जिसमें भारत-बांग्लादेश की वक्र सीमा को संज्ञान में लिया गया। कोर्ट द्वारा अधिकतर बांग्लादेश के दावे को माना गया। ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गयी प्रतिकूल एंट्री के बावजूद भारत द्वारा उक्त फ़ैसले का सम्मान किया गया।
यदि भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद की तुलना भारत-नेपाल विवाद से की जाये, तो वह वास्तव में सुलझाने में सरल प्रतीत होता है, अगर दोनों ही ओर से इसे सुलझाने के लिए राजनैतिक साख व शासन कला का पूर्ण इस्तेमाल किया जाये। आगे की प्रगति हेतु दोनो ही देशों को पट्टी नक्शों को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना, दो बचे हुए मामलों को सुलझाना, सम्पूर्ण भारत-नेपाल सीमा को विभाजक रेखा से निर्धारित करना व शीघ्रता से सीमा रखरखाव करना आवश्यक है।
अद्वितीय संबंध
भारतीय नेतृत्व नेपाली जनता के आत्म सम्मान व गौरव को लेकर पूर्ण रूप से सचेत है। जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ‘भारत की खोज’ (डिस्कवरी ऑफ इंडिया) व विश्व इतिहास की झलक (ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री) में वास्तविकता में नेपाल को दक्षिण एशिया का एकमात्र स्वतंत्र देश कहा था। नेपाल ने भी, भूतकाल में भारत की ज़रूरतों को एक मित्रतापूर्ण पड़ोसी के रूप में समझा है व उपयुक्त साथ दिया है। उसके राजनैतिक नेताओं द्वारा भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात केवल एक बार भारतीय ज़मीं पर विदेशी सेना को तैनात किया गया, जो कि सन 1948-49 में जनरल शारदा शमशेर के नेतृत्व में उत्तरी छावनी में नेपाली सेना के जवान थे, जब भारतीय सेना को कश्मीर व हैदराबाद में लगाया जाना पड़ा था।
नेपाली व भारतीय नागरिकों के बीच के संबंद्ध बहुत ही अहम रहे हैं। भारत के कईं कोनो में कभी कभी स्थानीय और दूसरे राज्यों के लोगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन शायद ही ऐसा कभी नेपाल के लोगों के विरुद्ध देखने व सुनने को मिलता है।
भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ़ जनरल मुकुंद नरवणे द्वारा इंस्टिट्यूट फ़ॉर डिफेन्स स्टडीज एंड एनालिसिस की एक चर्चा में यह कहना कि नेपाल द्वारा लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सड़क पर आपत्ति किसी अन्य देश (चीन) के कहने पर उठायी जा रही है, कहना उपयुक्त नहीं था। ऐसा कहने से अन्य ताकतों के लिए अड़चने खड़ी करने के मौके उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के विवादों को शांति से, द्विपक्षीय रूप से सुलझाना ही ठीक होता है।
विदेश मंत्रालय के अधकृत प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव द्वारा हाल ही में यह कहा गया है कि भारत व नेपाल द्वारा सभी सीमा संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि भारत, सीमा समस्याओं को राजनयिक वार्ता के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबध्द है। इसका मुख्य कारण भारत व नेपाल के बीच की करीबी मैत्री की भावना है। इस वक्त सबसे अहम कदम मौजूदा तन्त्र को सक्रिय करना होगा, इससे पहले की कोई और क्षति आगे हो।
जितने ज़्यादा समय तक परेशानियां दोनो देशों के बीच रहेंगी, उतनी ही ज़्यादा कुछ अन्य देशों को दोनों के बीच बिगड़ते संबंधों से फायदा होने के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय यह आवश्यक है कि दोनों देश तापमान को कम कर मामले को शांत करें। दोनों को ही समय व प्रयासों में निवेश करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक रूप से विवादों को बढ़ाना दोनों के ही लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
(जयंत प्रसाद पूर्व में नेपाल में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। यह लेख मूल रूप से ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित हुआ था।)