
पूरी मानवजाति इस समय एक वैश्विक संकट का सामना कर रही है । शायद हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट है ये । अगले कुछ हफ़्तों में लोग और सरकारें जो भी फैसले लेंगी, उनका प्रभाव आने वाले कई सालों तक इस दुनिया पर रहेगा। ये फैसले न सिर्फ हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देंगे बल्कि इनका प्रभाव अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति पर भी पड़ेगा । हमें जल्दी और दृढ़ता से फैसले लेने हैं और उन फ़ैसलों के दूरगामी परिणामों को भी ध्यान में रखना है । जब भी दो विकल्पों में से एक को चुनना पड़े तो अभी के खतरे से लड़ने के बारे में सोचने के साथ साथ ये भी सोचना है कि इस खतरे के टल जाने के बाद हम कैसी दुनिया में रहना चाहते हैं । हाँ, एक न एक दिन ये खतरा टल जाएगा, और मानवजाति फिर भी ज़िंदा रहेगी । हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदा होंगे लेकिन हमारी दुनिया बदल चुकी होगी ।
आपातकालीन परिस्थितियां ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं । सामान्य दिनों में जिन फ़ैसलों को लेने में सालों लगते हैं, वे चंद घंटो में ही ले लिए जाते हैं । कभी कभी खतरनाक और अपरिपक्व टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल शुरू हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में कुछ ना कर पाना शायद ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है । बड़े स्तर के सामाजिक प्रयोगों में पूरे-पूरे देश गिनी पिग बन जाते हैं । आज सभी घर से काम कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज का काम भी इंटरनेट से ही हो रहा है । सामान्य समय में सरकारें या शिक्षा से जुड़े लोग ऐसा करने के बारे में सोचते भी नही। लेकिन ये कहाँ कोई सामान्य समय है ।
इस संकट के समय में भी हमे चुनना है । हमारे पास दो विकल्प हैं । हम सर्वसत्तात्मक निगरानी चाहते हैं या नागरिकों का सशक्तिकरण? हम राष्टवादी अलगाव चाहते हैं या वैश्विक एकजुटता? कौन सा विकल्प ठीक होगा?
सर्वसत्तात्मक निगरानी
इस महामारी को रोकने के लिए पूरी आबादी को नियमों का पालन करना होगा और यह दो तरीके से हो सकता है ।
पहला तरीका है कि सरकार लोगों पर कड़ी निगरानी रखे और जो नियम तोड़ रहे हैं उनको सजा दे । मनुष्य के इतिहास में आज पहली बार टेक्नोलॉजी कि वजह से हर किसी पर हर समय निगरानी रख पाना संभव है । कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई सरकारों ने निगरानी रखने के नए-नए तरीके अपना लिए हैं । सबसे प्रसिद्ध मामला तो चीन का ही है । स्मार्ट फ़ोन पर निगरानी और चेहरा पहचान लेने वाले कैमरा की मदद से और लोगों के लिए अपनी सेहत की जानकारी देना अनिवार्य करके चीन सरकार ना केवल कोरोना वायरस के मरीज़ की पहचान कर पा रही है बल्कि ये मरीज़ किस किस से मिल चुके हैं इसका भी पता लगा रही है । ऐसी कई मोबाइल एप्लीकेशन्स भी हैं जो लोगों को आगाह कर देती हैं जब वे किसी मरीज़ के नज़दीक होते हैं ।
इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ पूर्वी एशिया तक ही सीमित नही है । इजराइल के प्रधान मंत्री ने वहाँ के सुरक्षा मंत्रालय को कोरोना वायरस के मरीज़ों पर निगरानी रखने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दे दी है जो सामान्य दिनों में आतंकवादियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है । जब उचित संसदीय उपसमिति ने ऐसा करने की मंज़ूरी नही दी तो वहाँ के प्रधान मंत्री ने आपातकालीन डिक्री लगाकर इसे मंज़ूर करवा दिया ।
अब आप बोलेंगे कि इसमें कुछ भी नया नही है । आज के समय में सरकारें और बड़े व्यापारसंघ अपने फायदे के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों पर निगरानी रख ही रहे हैं । लेकिन फिर भी अगर हम सावधान नही रहे तो यह महामारी का समय सर्वसत्तात्मक निगरानी के इतिहास में एक भयानक समय साबित हो सकता है । निगरानी रखने के साधन जिनको आज तक हमने अस्वीकार किया है, वे आज के समय में हमारे लिए आम बात बन सकते हैं । पहले सरकारों को यह जान ने में दिलचस्पी थी कि हम फ़ोन पर कौन सा लिंक खोल रहे हैं और क्या देख रहे हैं, अब वे हमारा तापमान और ब्लड प्रेशर भी जान ना चाहेंगे ।
संकट का फायदा
समस्या यह है कि हमें पता नही है कि हमारे ऊपर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है और आने वाले समय में क्या होगा । निगरानी रखने वाली टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जो कल कहानी था वो आज का सच बन चुका है । ज़रा सोचिये अगर सरकार आपको हाथ में एक ऐसा कड़ा पहनने के लिए कहे जिससे आपके शरीर के तापमान और हार्ट रेट पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जा सके तो आपसे पहले सरकार को आपकी बीमारी का पता होगा । महामारी को फैलने से रोकना कितना आसान हो जाएगा । अच्छा आईडिया है ना? इसमें बुरा क्या है ?
बुरा यह है कि ऐसा करने से एक भयानक निगरानी रखने कि व्यवस्था को वैद्यता मिल जाएगी । अगर आपको सिर्फ यह पता है कि मै NDTV का लिंक ज़्यादा खोल रही हूँ या Zee News का तो आपको सिर्फ मेरे राजनीतिक विचारों के बारे में पता चलेगा लेकिन अगर किसी वीडियो को देखते समय आप मेरे तापमान, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी नाप सकते हैं तो आप को यह भी पता चल जाएगा कि क्या देख के मैं हँसता हूँ, क्या देख के रोता हूँ और किस बात से मुझे गुस्सा आता है ।
यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि गुस्सा, ख़ुशी, उदासी, प्यार भी उतना ही जैविक है जितना कि बुखार या खांसी । एक टेक्नोलॉजी जो आपकी खांसी का पता लगा सकती है, वह आपकी हंसी भी पहचान सकती है । अगर सरकारें और बड़े व्यापारसंघ हमारा बायोमेट्रिक डाटा निकलने लग गए, तो जितना हम खुद को जानते हैं उससे बेहतर वे हमे जान जाएंगे । उनको ना सिर्फ हमारी भावनाओं का पता पहले से चल जाएगा बल्कि वे अपने फायदे के अनुसार उसे बदल भी पाएंगे । उनके लिए फिर हमे कुछ भी बेचना मुश्किल नहीं होगा चाहे वह कोई सामान हो या फिर कोई राजनेता । एक ऐसी काल्पनिक दुनिया के बारे में सोचिये जहाँ ये सब कुछ हो रहा हो और आपके हाथ में बायोमेट्रिक कड़ा हो । ऐसे में अगर आपको किसी बड़े राजनीतिज्ञ का भाषण सुनकर गुस्सा आ गया और उस कड़े ने यह भांप लिया तब तो आप गए काम से ।
आप यह कह सकते हैं कि यह बायोमेट्रिक निगरानी सिर्फ अभी के संकट के लिए है । एक बार संकट टल गया तो इसका इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा । पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कोई न कोई संकट हमेशा आता ही रहता है । कोरोना वायरस ख़त्म भी हो गया तो सरकारें बोल सकती हैं कि बायोमेट्रिक निगरानी चाहिए क्योंकि यह वायरस दोबारा आ सकता है । या फिर एबोला वायरस आ सकता है या फिर कुछ और । बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है । कुछ सालों से हमारी प्राइवेसी (निजता) पर खतरा मंडरा ही रहा है जो कि कोरोना वायरस के चलते बहुत बढ़ सकता है क्योंकि अगर लोगों को सेहत और निजता के बीच में चुनना पड़ा तो वह सेहत को ही चुनेंगे ।
दरअसल समस्या की जड़ यही है कि लोगों को निजता और सेहत के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है, जो कि गलत है । हमें सेहत और निजता दोनों मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए । हम कोरोना वायरस महामारी को सर्वसत्तात्मक निगरानी की बजाय नागरिकों के सशक्तीकरण से भी हरा सकते हैं । पिछले कुछ हफ़्तों में इस महामारी पर सबसे बेहतरीन तरीके से काबू करने वाले देश हैं – ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर । इन देशों ने सिर्फ कुछ हद तक ही ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है । इनकी सफलता के प्रमुख कारण है – ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच (टेस्टिंग) करना, ईमानदारी से जनता को सही समाचार देना और एक जागरूक जनता का भरपूर सहयोग मिलना ।
निगरानी रखना और कड़ी सजा देना ही सिर्फ एक तरीका नहीं है लोगों से नियम पालन करवाने का । जब आप लोगों को सच बताएंगे, वैज्ञानिक तथ्य बताएंगे और जब जनता को उनके राजनीतज्ञों और नेताओं पर भरोसा होगा तब वह अपने आप ही नियमों का पालन करेगी । स्वतः प्रेरित और जागरूक जनता, मूर्ख और बंदिश में रखी हुई जनता से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है । लेकिन लोगों से अनुपालन और सहयोग सिर्फ तभी मिलता है जब लोगों को भरोसा हो राजनीतिज्ञों पर, मीडिया पर और विज्ञान पर । पिछले कुछ सालों में, कुछ गैर ज़िम्मेदार राजनीतिज्ञों की वजह से हमारा भरोसा विज्ञान, मीडिया और राजनीति पर कमज़ोर हो चुका है । और अब यही गैर ज़िम्मेदार राजनीतिज्ञ यह बोलते हैं कि जनता पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसलिए अधिनायकवाद या तानाशाही कि ज़रुरत है ।
जिस भरोसे को नष्ट करने में सालों लगे हैं, सामन्यतः वह रातों रात तो वापस नहीं आ सकता । लेकिन फिर यह कोई सामान्य समय भी तो नहीं है । किसी परेशानी के समय में मन बदलने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती । अपने भाई या बहन से चाहे सालों कि नाराज़गी हो लेकिन किसी आपातकालीन समय में आप दोबारा उन पर भरोसा करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनकी मदद भी करेंगे । इसी तरह जनता का भरोसा भी वापस जीतने के लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है, यह मुमकिन है । टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए पर एक आम नागरिक को सशक्त करने के लिए । मैं बायोमेट्रिक डाटा लेने के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन इसका प्रयोग सरकारों को अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए । इस डाटा से तो मुझे मदद मिलनी चाहिए कि मैं ज़्यादा बेहतर चीज़ें चुन सकूं और सरकार को उनके लिए हुए फैसलों के लिए ज़िम्मेदार ठहरा सकूं ।
कोरोना वायरस महामारी हमारी नागरिकता का इम्तिहान है । आगे आने वाले दिनों में हमे यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वैज्ञानिक डाटा और एक्सपर्ट्स पर विश्वास करें, ना कि अफवाहों पर और आत्म सेवारत राजनीतिज्ञों पर । अगर हमने अभी सही चुनाव नहीं किया तो हम अपनी बहुत सारी आज़ादियाँ खो बैठेंगे, ये सोच के कि सिर्फ यही एक तरीका है अपने आप को स्वस्थ्य रखने का।
हमें एक वैश्विक योजना की ज़रूरत है
दूसरा महत्त्वपूर्ण चुनाव हमें करना है राष्ट्रवादी अलगाव और वैश्विक एकजुटता के बीच । महामारी और उसकी वजह से आने वाला आर्थिक संकट दोनों ही वैश्विक समस्याएं हैं । इनका समाधान सिर्फ वैश्विक सहयोग से ही हो सकता है ।
सबसे पहली बात यह है की इस वायरस को हराने के लिए हमे पूरे विश्व से जानकारियाँ साझा करनी होंगी । वायरस यह नहीं कर सकता लेकिन हम तो कर सकते हैं । चीन का वायरस अमेरिका के वायरस को इंसानों को संक्रमित करने की टिप्स नहीं दे सकता । लेकिन चीन अमेरिका को कोरोना वायरस से लड़ने के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक दे सकता है । सुबह की गई इटली के डॉक्टर की खोज शाम को तेहरान में किसी की ज़िन्दगी बचा सकती है । अगर ब्रिटेन को नीतियां बनाने में दिक्कत हो रही हो तो वह कोरिया की मदद ले सकता है जिसने एक महीने पहले शायद ऐसी ही नीतियों पर काम किया होगा । लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर एक वैश्विक सहयोग और विश्वास की भावना हो ।
सभी देशों को आगे बढ़कर ईमानदारी से जानकारियां साझा करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी लेनी चाहिए । ऐसा होने पर दूसरे देशों द्वारा साझा की गयी जानकारियों पर हम भरोसा भी कर पाएंगे । पूरे विश्व को मिलकर प्रयास करना होगा टेस्टिंग किट और चिकित्सा से जुड़ी मशीनें बनाने का । सब कुछ खुद बनाने या जो हमारे पास है उसकी जमाखोरी करने से बेहतर होगा कि पूरा विश्व समन्वित तरीके से ये मशीने बनाये । इस तरह से शायद सबकी ज़्यादा मदद हो पाएगी । हमे यह लड़ाई मानवता के साथ लड़नी होगी और सभी देशों को एक दूसरे की मदद भी करनी होगी ।
वैश्विक सहयोग की ज़रूरत आर्थिक संकट से उबरने के लिए भी है । आर्थिक व्यवस्था एक वैश्विक व्यवस्था है और अगर सभी देश सिर्फ अपना अपना देखेंगे तो यह संकट कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा । हमें एक वैश्विक योजना बनानी होगी और जल्दी बनानी होगी ।
पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे निष्क्रिय सा हो गया है । कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है । २००८ के आर्थिक संकट में या २०१४ की इबोला महामारी में अमेरिका एक वैश्विक नेता की भूमिका में था । लेकिन अमेरिका के आज के रवैये से यह साफ हो गया है कि वह सिर्फ खुद की महानता की फ़िक्र करता है, मानवता के भविष्य की नही। अमेरिकी शासन ने अपने सबसे करीबी सहयोगी दलों को भी अकेला छोड़ दिया है । यूरोप से सभी यात्राएं प्रतिबंधित करने से पहले अमेरिका ने यूरोप को पहले से बताने की भी ज़रूरत नही समझी । अमेरिका ने जर्मनी की फार्मा कंपनी को एक बिलियन डॉलर देने की कोशिश की ताकि वह कोरोना वायरस की वैक्सीन का एकाधिकार खरीद सके । अगर अभी अमेरिका अपना रवैया बदल भी ले तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो एक ऐसे नेता के पीछे चलना चाहेंगे जो ज़िम्मेदारी ना लेता हो, कभी अपनी ग़लतियाँ ना मानता हो और श्रेय खुद लेता हो और ग़लतियाँ दूसरों पर डालता हो ।
अगर अमेरिका की जगह आज कोई और देश नेतृत्व की भूमिका नही ले पाया तो इस महामारी को ना सिर्फ रोकना मुश्किल होगा बल्कि इस महामारी की विरासत आने वाले कई सालों तक अंतराष्ट्रीय संबंधों में ज़हर घोलती रहेगी । हर संकट एक अवसर भी होता है । हमें उम्मीद करनी चाहिए की यह महामारी पूरी मानवता को ये एहसास दिलाएगी की वैश्विक एकजुटता का अभाव होना कितने बड़े संकट को जन्म दे सकता है ।
हमें चुनना होगा वैश्विक एकता और राष्टवादी अलगाव के बीच । अलगाव से ना सिर्फ ये संकट देर तक रहेगा बल्कि आने वाले समय में यह अलगाव इससे भी बड़े संकटों को जन्म देगा । वैश्विक एकजुटता से हम कोरोना वायरस के साथ साथ आगे आने वाले इक्कीसवी सदी के और भी गंभीर संकटों को हरा पाएंगे।
यह लेख मौलिक रूप से अंग्रेजी में प्रथम बार Financial Times में प्रकाशित हुआ था ।
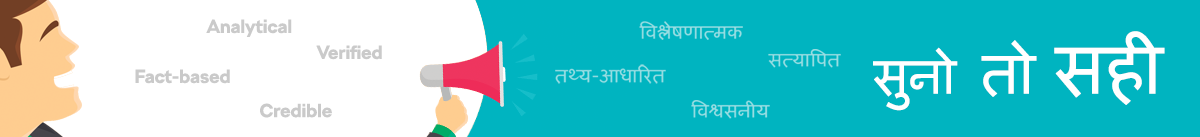


Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.